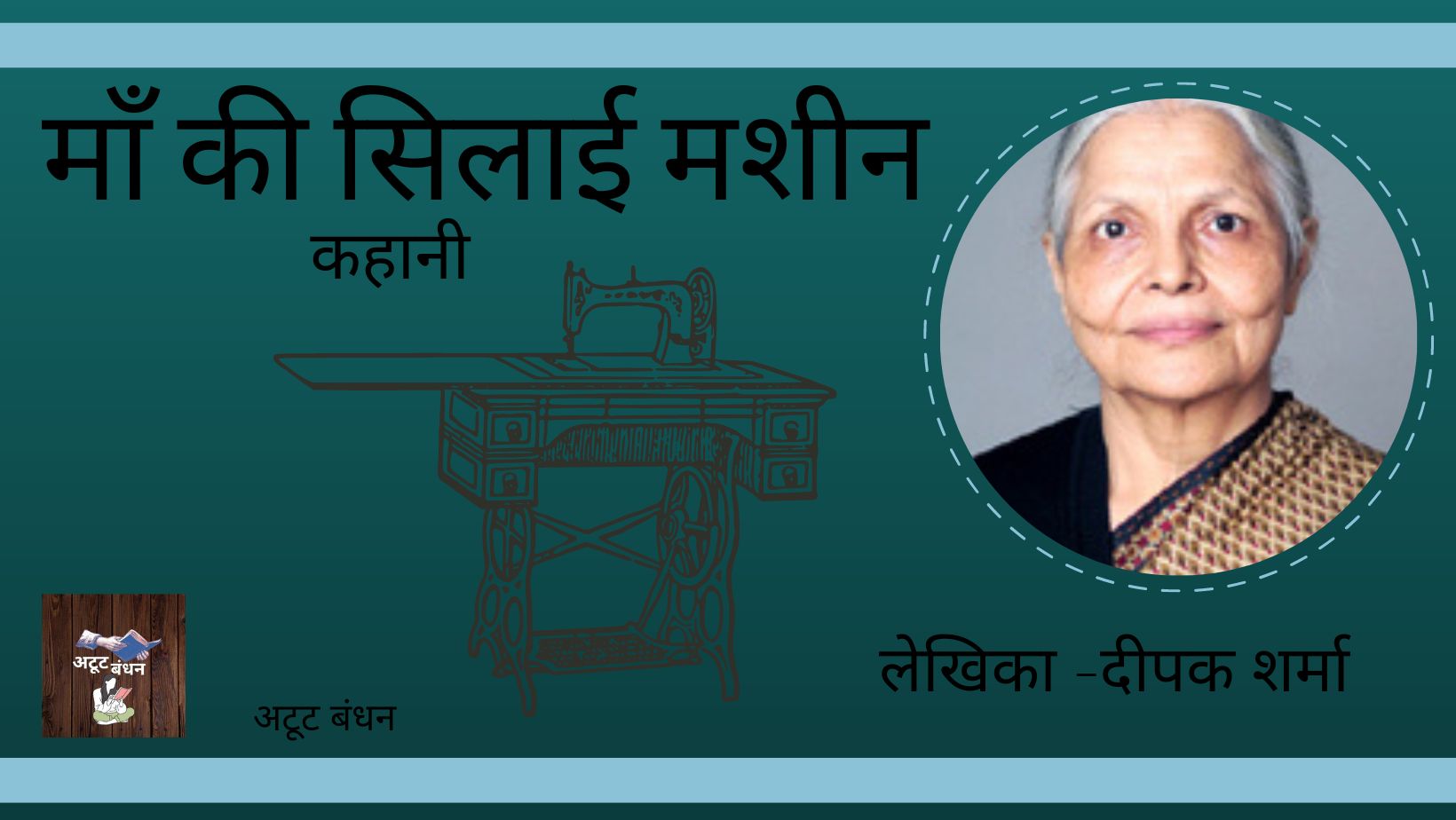दीपक शर्मा की कहानी एवज़ी
वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानियाँ पढ़ते हुए बिहारी का ये दोहा अनायास ही जुबान पर आ जाता है l सतसइया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर, छोटी सी कहानी ‘एवजी’ भी मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों की सेवा टहल के लिए अपनी सेवाएँ देने वालों के ऊपर … Read more